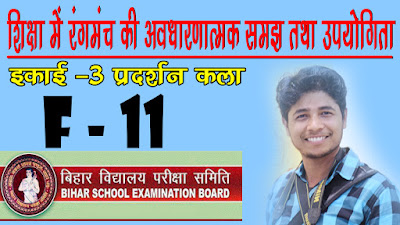आत्म की समझ
आत्म (स्वयं) एक ऐसा आकर्षण का केंद्र है जिसके इर्द-गिर्द (आस-पास) अनेक आवश्यकताएं और लक्ष्य संगठित होते हैं। और आत्म (Self) दूसरों मनुष्य के संबंध में विचारों और कार्यों की चेतना है। आत्म से अभिप्राय है:- स्वयं के प्रति दृष्टिकोणो के विकास का परिणाम।
एक मनुष्य स्वयं की पहचान यह कह कर कर सकता है कि, "मेरा घर", "मेरी पाठशाला", "मेरा परिवार", "मेरी जाती", "मेरे मित्र", इत्यादि। यह सभी बातें उसके अहम् के दृष्टिकोण को दर्शाती है। व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है । यह आपस में जुड़े आत्म के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति के व्यवहार में स्थिरता लाता है। व्यक्ति के विभिन्न दृष्टिकोणो में एक विशेष संबंध होता है। आत्म विकासात्मक प्रक्रिया है। जिसमें दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण भी शामिल होते हैं यह एक विकासात्मक प्रतिफल है।
क्रेचफील्ड के अनुसार,
आत्म वह एक तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है।
जेम्स ड्रिक्ट के अनुसार,
आत्म शब्द का प्रयोग अहम् के अर्थ में किया जाता है। उसके अनुसार आत्म सामान्यत: अहम के अर्थ में एक घटक के रूप में जाना जाता है जो अपनी पहचान की निरंतरता के लिए चेतन रहता है।
यंग के अनुसार,
आत्म को हम वैसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जैसे वह अपने को अंतः क्रिया के संदर्भ में स्वयं देखता या जानता हो।
आत्म शब्द का प्रयोग किसी एक व्यक्ति की क्रियाओं और व्यवहारों के कुल जोड़ के लिए किया जाता है । यह इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि कोई व्यक्ति व्यवहार की दृष्टि से क्या है। व्यक्ति के आत्म में वह सब कुछ शामिल होता है जिसे वह अपना कह सके।आत्म वह है जिससे हम परिचित हैं। आत्म व्यक्ति के स्वयं के प्राप्त अनुभव से निर्मित होता है। यह व्यक्ति का आंतरिक संसार है। यह व्यक्ति के विचारों और भावनाओं, आशाओं और निराशाओं, भय और कल्पनाओं एवं उसका स्वयं के प्रति विचार कि वह क्या है? वह क्या था? वह क्या बन सकता है? और उसका स्वयं के बारे में क्या दृष्टिकोण है।
व्यक्ति की स्वयं के प्रति अभिवृत्ति (Aptitude, Attitude) के ज्ञानात्मक पहलू का अर्थ आत्म की विषय वस्तु से है।
जैसे:- मैं लंबा हूं, मैं सुंदर हूं, मुझे सब कुछ आता है। इत्यादि। इसी प्रकार के स्वयं के प्रति अभिवृत्ति के भावनात्मक पहलू का अर्थ उन भावनाओं से है जो व्यक्ति अपने स्वयं के प्रति रखता है।
"यह कार्य मैं कर सकता हूं। यह हुआ आपका ज्ञान।
लेकिन यह कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूं यह हो गया आपका अभिमान।।
इन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना कठिन कार्य होता है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार
आत्म जन्मजात नहीं होता यह सामाजिक स्थितियों की क्रिया का अर्जित परिणाम है।
जैसे भोजपुरी में एक कहावत है-
संगत से गुण आवत है, औऱ संगत से गुण जात।
स्वयं की अवधारणा से तात्पर्य (Meaning of the Concept of Self):- व्यक्ति स्वयं के बारे में जो सोचता है तथा अपने बारे में जो अवधारणा विकसित करता है उसे ही हम स्वयं की अवधारणा (concept of self) कहते हैं।
इसे हम लोग दो रूपों में विभाजित कर सकते हैं-
- वास्तविक स्वम् (Real Self)
- आदर्शात्मक स्वम् (Ideal Self)
वास्तविक स्वमं का तात्पर्य होता है व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है। जैसे वह कौन है? उसमें क्या-क्या विशेषताएं हैं? इत्यादि। आदर्शत्मक स्वयं का अर्थ होता हैं। वह कैसा होना चाहता है? तथा आगे चलकर कैसा बनना चाहता है? इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयं के दोनों रूपों में से प्रत्येक का संबंध शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों पहलूओ से होता है। शारीरिक दृष्टिकोण में शारीरिक अनुभव एवं शारीरिक क्षमता तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में बुद्धि कौशल एवं अन्य लोगों के साथ मानसिक क्षमताओं का प्रदर्शन इत्यादि से स्वयं संबंधित होता है।
व्यक्तित्व के विकास में अनुवांशिक कारक (Hereditary Factors) तथा परिवेशीय कारक (Environmental Factors) दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि अनुवांशिकता तथा पर्यावरण के बीच सही ढंग से समायोजन (Adjustment) स्थापित नहीं होगा तो व्यक्तित्व का विकास होना असंभव होता है। व्यक्तिगत अनुभव भी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं।
स्वयं का विकास ( The Development of Self):- स्वयं के विकास में सामाजिकीकरण (Socialization) की अहम भूमिका होती है। बच्चों के प्रारंभिक स्वयं के स्वरूप पर माता-पिता तथा सहोदरों (Siblings) का अधिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वे प्रारंभिक वर्षों में उन्हीं के संपर्क में सर्वाधिक रहते हैं। जिस बालक के छोटे भाई-बहन होते हैं। उनकी भूमिका परिवार में एक जिम्मेदार बालक की हो सकती है। इसका भी प्रभाव बालक के स्वयं के विकास (Development of self) पर पड़ता है। बालक जब विद्यालय में प्रवेश करता है तब उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है। बालक को विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों एवं घटनाक्रमों के प्रति अभिवृत्तिया (Expressions) उन अभिवृत्तियों से प्रभावित होती है जो उसके जीवन में प्रमुख अभिकर्ता (Main Agent) जैसे:- शिक्षक, माता-पिता, पड़ोसी, मित्र, आदि के रूप में होते हैं।
स्वयं के बारे में एक दार्शनिक दृष्टिकोण (Philosophical perspective towards Self):- स्वयं के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण विचार या परिपेक्ष्य है वह है अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य (Existential Perspective) यह परिपेक्ष्य व्यक्ति के विचारों एवं व्यवहार पर बल देता है। इसकी विशेष रूचि व्यक्ति के स्वयं में, स्वयं के मूल्यांकन में, भावनाओं (Emotions) एवं संवेदनाओं (Condolences) के अध्ययन में होता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के सारे विचार और सिद्धांत उसके चिंतन का ही परिणाम है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपना सिद्धांत स्वयं खोजना या बनाना चाहिए। दूसरों के द्वारा निर्मित या प्रतिपादित सिद्धांतों को स्वीकार करना उसके लिए आवश्यक नहीं होता।
संसार को स्वयं की अभिव्यक्ति कभी नहीं समझना चाहिए, ना ही संसार को एक मात्र साधन या आत्मपरिचय को प्राप्त करने का उपाय। इससे यही आशय स्पष्ट होता है कि जीवन का अर्थ स्थिर नहीं है और ना ही इसका कोई किनारा। हम जीवन के अर्थ को तीन तरीकों से ढूंढ सकते हैं-
- कर्म के माध्यम से
- किसी के या किसी वस्तु के मूल्य को अनुभव करके
- पीड़ा से
जीवन के अर्थ को पहले तरीके से पूर्ण करना अत्यंत लाभदायक होता है। दूसरे तरीके के द्वारा जीवन में अर्थ का प्रवेश होता है। और वो अनुभव से ही प्राप्त होता है। यह शिक्षा हमें प्रकृति से, संस्कृति से या फिर किसी को अनुभव करके, अनुभव करना यानी प्रेम के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तीसरा तरीका जो मनुष्य को अपने जीवन के अर्थ को खोजने में सहायता करता है वह है, पीड़ा। मनुष्य जब भी असहाय या ऐसी परिस्थिति से गुजरता है जिसका परिणाम उसके हाथ में ना हो । जैसे:- कोई लाइलाज बीमारी। उसी वक्त एक इंसान को अपनी पहचान को बोध करने का भरपूर मौका मिलता है। अर्थात कष्ट को झेलकर ही जीवन का सबसे बड़ा अर्थ पाने का अवसर प्राप्त होता है।
स्वयं के बारे में एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण(Cultural Perspective towards Self):- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह कथन महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु का है अरस्तू प्लेटो के शिष्य थे एवं सिकंदर के गुरु भी थे।मानव समूहों के बीच रहता है। विश्व के समस्त जीवधारियों में केवल यही संस्कृति का निर्माता है कोई भी संस्कृति प्रकृति प्रदत नहीं होती यह मानव समाज के द्वारा ही निर्मित होती है। संस्कृति स्वयं (self) के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि में सकारात्मक परिवर्तन भी लाती है यह हमारे धार्मिक कार्यों में, मनोरंजन में, वर्ग संचालन एवं ज्ञान प्राप्त करने में और आनंद प्राप्त करने के तरीकों में भी देखी जा सकती है।
संस्कृतिया व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है। सांस्कृतिक वातावरण (Cultural Environment) में भिन्नता के कारण लोगों के आचार-विचार में भी भिन्नता आ जाती है। जिस संस्कृति की जैसी मान्यता तथा विचारधारा होगी उसमें पोषित लोगों में उसी प्रकार के गुणों का विकास भी होता है। व्यक्तित्व संस्कृति का दर्पण होता है। सांस्कृतिक मान्यताओं का ही परिणाम है कि कुछ समाज के व्यक्ति अधिक धर्मार्थ, शांत और विनम्र होते हैं। जबकि कुछ समाज के सदस्य ईर्ष्यालु एवं आक्रामक होते हैं। सांस्कृतिक तत्वों का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर बड़े ही विचित्र ढंग से पड़ता है।
कबीर के दोहे
उज्जल बूंद आकाश की,
परी गई भूमि विकार।
माटी मिली भई कीच सो,
बिन संगति भौउ छार।।
अर्थात, आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें निर्मल और उज्जवल होती है किंतु जमीन पर गिरते ही गंदी हो जाती है। मिट्टी में मिलकर वह कीचड़ हो जाती है इसी तरह मनुष्य भी अच्छी संगति के अभाव से बुरा हो जाता है।
चन्दन जैसे संत हैं,
सरूप जैसे संसार।
वाके अंग लपटा रहै,
भागै नहीं विकार।।
अर्थात, संत चन्दन की भांति होते हैं और यह संसार सांप की तरह विषैला है। किंतु सांप यदि संत के शरीर में बहुत दिनों तक लिपटा रहे तब भी सांप का विष-विकार समाप्त नहीं होता है।